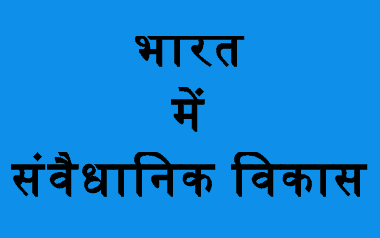संवैधानिक विकास
संविधान लिखित व अलिखित नियम-कानूनों का ऐसा दस्तावेज है। जिसके माध्यम से शासन और जनता के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। ब्रिटिश संविधान अलिखित होते हुए भी संविधान की शर्तों को पूरा करता है।
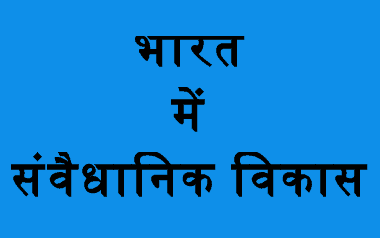
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आयी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापारियों के एक समूह को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया।
1609 ई. में इस अधिकार पत्र को स्थायित्व प्रदान किया गया। समय-समय पर इस अधिकार पत्र में 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापार क्षेत्र में वृद्धि की गई। 1661, 1669, 1677 के एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करते हुए न्याय प्रशासन और दीवानी मामले कंपनी को सौंप दिए गए इस एक्ट के द्वारा एक प्रावधान यह भी किया गया कि कंपनी का प्रशासन एक गवर्नर और 24 सदस्यों के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम दिया गया।
1726 और 1753 के राज लेख द्वारा इस कंपनी के अधिकार क्षेत्र में व्यापक व्यक्ति करते हुए कोलकाता मुंबई और मद्रास का प्रेसीडेंसी के रूप में पुनर्गठन किया गया। 1765 में कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अधिकार तथा लगान वसूलने के अधिकार प्राप्त किए,परंतु फौजदारी विषयों का प्रशासन और उत्तरदायित्व अब भी नवाब के हाथों में बना रहा। (यह व्यवस्था कालांतर में 1772 तक द्वैध शासन के रूप में चलती रही)
1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक प्रकारों के व्यवहारों ने दो विपरीत प्रकार की स्थितियों को जन्म दिया।
- 1769 व 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में अकाल के कारण भारी मात्रा में क्षति हुई।
- 1770 ईस्वी में भारत से लूटे गए धन की बदौलत इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ।
इस स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने से ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की गई। इस मांग के परिणामस्वरुप ब्रिटिश सरकार का कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने पर जो अवसर प्राप्त हुआ उसी का परिणाम था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम एक्ट कहा जाता है।
ब्रिटिश शासन को हम दो प्रकार से देखेंगे
- 1⃣ कंपनी का शासन- (1773 से 1858)
- 2⃣ताज का शासन – (1858 से 1947 तक)
1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा. इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं. वे निम्न हैं:
कंपनी का शासन (1773 से 1758)
1. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ( Regulating Act of 1773 )
1773 रेगुलेटिंग एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार कंपनी के प्रशासन के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया यह लिखित संविधान प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रयास था।
रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
विशेषताएँ
- रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया( यह सदस्य सम्राट के द्वारा नियुक्त थे और कंपनियों के कर्मचारी नहीं मानेंगे) जिसके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
- परिषद में सभी निर्णय बहुमत से होते थे और गवर्नर जनरल उन निर्णय से बाह्य था।
- बंगाल की आर्थिक स्थिति और विशालकाय क्षेत्रफल के कारण बंगाल को मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी पर सर्वोच्चता प्रदान की गई। बंगाल का गवर्नर इन तीनों प्रेसिडेन्सियों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा,जो वारेन हेस्टिंग्स था। इससे पहले सभी प्रेसिडेसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे।
- रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। उसके अधिकार क्षेत्र में गर्वनर और उसकी परिषद के कार्य शामिल थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया।
- समिति का गठन ब्रिटेन से लिया गया।यह विचार कालांतर में न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्णगामी साबित हुआ।
- रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में उपलब्ध राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
- तत्कालीन वायसराय लार्ड नार्थ द्वारा गठित गुप्त समिति द्वारा पारित. कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार लिखित संविधान का प्रावधान
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष की स्थान पर 4 वर्ष का नाम करना , कुल सदस्य 24
- 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे
2. 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट
- इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किए गए इसलिए इसे संशोधनात्मक एक्ट कहते हैं
3. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
रेग्यूलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिये इस एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया।
इस एक्ट के प्रमुख उपबंध निम्नानुसार थे
इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल )नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया
इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया |
नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी की वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक , सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे
- अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों के लिए प्रथम वैज्ञानिक दस्तावेज
- शीर्षक :भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र।
- कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को अलग अलग करना (बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 सदस्य )राजनीतिक कार्य तथा (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) व्यापारिक कार्य
- गवर्नर जनरल की सदस्य संख्या 4 से 3 करना
- प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को देना
- कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाना
यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था
- 1. भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया
- 2. ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया
4. 1793 का चार्टर एक्ट
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था करना
- ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्रों में द्वारा लिखित विधियों द्वारा शासन की शुरुआत
- न्यायालय को सभी कानून और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया
5. 1813 ई. का चार्टर अधिनियम:
अधिनियम की विशेषताएं
- कंपनी के अधिकार-पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया
- कंपनी के भारत के साथ व्यापर करने के एकाधिकार को छीन लिया गया. लेकिन उसे चीन के साथ व्यापर और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया.
6. 1833 ई. का चार्टर अधिनियम:
ब्रिटिश भारत के केन्द्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था |
अधिनियम की विशेषताएं
- कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया
- बंगाल के गवर्नर जरनल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा.जिसमे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी
इस प्रकार इस अधिनियम में एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो
लार्ड विलिअम बैंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे - इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया |भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए | इसके अन्तर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया
- भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई.
7. 1853 का चार्टर अधिनियम
1813 के अधिनियम की समीक्षा के उद्देश्य से जो अधिनियम 1833 में आया वह अब तक का सर्वाधिक उदार एवं महत्वपूर्ण अधिनियम था 1853 एक्ट में पहली बार भारत में वैधानिक दृष्टि से सुधारों का दौर आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी गई।
1833 के एक्ट में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लार्ड मैकाले थे। इस अधिनियम से सर्वप्रथम भारत में विधियों के संहिताकरण का आधार तैयार हुआ। इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंक थे। भारत गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गया। इसके अंतर्गत पहले बनाई गये कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा गया।
चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। 1833 अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 87 में मिलता है। जिसमें धर्म जाति वर्ग के आधार पर सेवाओं में सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
इस प्रावधान का प्रभाव भारतीय संविधान के भाग-3 अनुच्छेद 15 और 16 के मौलिक अधिकारों में दर्शाए गए हैं। इसी प्रावधान को 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भी देखा गया। इसी प्रावधान में पहली बार अधिनियम शब्द का इस्तेमाल किए जाने लगा। इससे पहले केवल विनियम (रेग्यूलेटिंग) शब्द का प्रयोग होता था।
1833 के एक्ट के पारित होने के पश्चात भारत के विभिन्न प्रांतों से यह मांग उठने लगी कि भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ब्रिटिश संसद में कंपनियों के अधिकारियों की आर्थिक समृद्धि को देखते हुए यह मांग की जाने लगी कि कंपनी का व्यापारिक प्रशासन और अधिक ना बढ़ाया जाए। इन मांगों के परिदृश्य में 1853 का एक्ट लाया गया।
1853 का एक्ट
1793 से 1893 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था ब्रिटेन की संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय भारत में कंपनी की शासन को समाप्त कर सकती हैं।
इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें भी एक तिहाई सदस्य सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाने लगे।
सम्राट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों का प्रावधान किया गया जिसमें दो न्यायधीश और चार व्यक्ति मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा से प्रांत से लिए गए।
1857 में स्वाधीनता संग्राम के पश्चात भारत में संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से लार्ड पार्मस्टर्न में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया। जिसमें यह घोषणा की गई की “असुविधाजनक कष्टकारी और हानिकारक व्यवस्था का अंत कर के नए प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाए।
यह विधेयक कानून पारित नहीं हो सका। लेकिन 2 अगस्त 1818 को भारत शासन अधिनियम के रूप में एक नई प्रकार की व्यवस्था ने जन्म लिया।
2. ताज का शासन {1858 से 1947 तक}
A. 1858 का भारत शासन अधिनियम
इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद किया गया। जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गर्वनरों,क्षेत्रों,राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दी गई।
इस अधिनियम से सर्वप्रथम द्वैध शासन का अंत किया गया। तत्कालीन समय में शक्ति के तीन केंद्र स्थापित थे।
- 1⃣गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद
- 2⃣बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
- 3⃣बोर्ड ऑफ कंट्रोल
इन सभी को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के रूप में एक नए पद का सृजन किया गया जिसे राज्य सचिव एवं भारत मंत्री कहा गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। जिसकी सहायता के लिए 15 व्यक्तियों की एक परिषद गठित की गई। जिसमें कम से कम आधे सदस्य सम्राट के द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने थे। जो भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा कर चुके हो।
इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था
संरक्षण-ताज, सपरिषद राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बंट गया। अनुबद्ध सिविल सेवा (covenanted civil service) में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगीं भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय (Corporate Body) घोषित किया गया, जिस पर इंग्लैंड एवं भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था।
B. 1861 इंडियन काउंसलिंग एक्ट
इस अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया।
इस अधिनियम को लाने का प्रमुख उद्देश्य विकेंद्रीकरण की प्रणाली को प्रारंभ करना था गर्वनर जनरल को अपनी परिषद की बैठक के समय एवं स्थान को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई अन्य प्रांतों में भी विधान परिषद के निर्माण की शक्ति दी गई। जिसके अंतर्गत 1862 में बंगाल में, 1886 में आगरा एवं अवध, 1897 में पंजाब में, 1818 में बर्मा में, 1912 में बिहार,उड़ीसा,असम में तथा 1913 में मध्य प्रांत में विधान परिषदों का निर्माण किया गया।
गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इसमें अध्यादेश की अवधि छ: माह होती थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली”(पोर्टफोलियो सिस्टम)” लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया। जिसमें शासन की सुविधा के लिए प्रशासन को कुछ विभाग भी बांटे जाने का प्रावधान किया गया।
इस एक्ट के माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की कोशिश की गई। जिसने भारत में राजनीतिक संगठनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जिसकी अभिव्यक्ति में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हिंदुओं और मुसलमानों का सांप्रदायिक विद्वेष प्रारंभ हुआ।
अधिनियम की विशेषताएं
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया,विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ,गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई.
- इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसीडेन्सियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की
- इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की |गवर्नर जरनल को बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई.
C. 1892 का भारत अधिनियम
1892 के अधिनियम के अंतर्गत विधायी परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 की गई। प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 से 50 सदस्यों के बीच में रखी गई। परिषद में सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिया गया।
इसने केंद्रीय विधान परिषद् और बंगाल चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था | इस व्यवस्था में निर्वाचन की पूर्व सूचना दिखाई दे रही थी जिसकी अभिव्यक्ति 1909 के अधिनियम में देखने को मिली।
Constitutional Development important facts
- प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल-लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स
- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल- लॉर्ड विलियम बैंटिक
- भारत के प्रथम वायसराय- लॉर्ड केनिंग
- साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक- लॉर्ड मिंटो
- डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल- लॉर्ड माउंटबेटन
संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास संवैधानिक विकास