प्राचीन प्रमुख राजवंश
कुषाण_वंश

कुषाण वंश मौर्योत्तर कालीन भारत का ऐसा पहला साम्राज्य था,
जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था।
यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर तत्कालीन विश्व के तीन बड़े साम्राज्यों रोम, पार्थिया एवं चीन के समकक्ष था।
कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत चीनी की पुस्तक history of the Han Dynasty, Analysis of Latter Han Dynasty
तथा भारतीय पुस्तकें नागार्जुन कृत माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष की बुद्धचरित हैं।
कुषाण पश्चिमी क्षेत्र के यूची जाति के थे। लगभज 165 ईसा पूर्व इसके पड़ोसी कबीले “हिंग नू” ने यूचियों के नेता को पराजित कर मार डाला।
यूचियों को पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह क्षेत्र छोड़ते समय यूची कबीला दो भागों में विभक्त हो गया।
पहला कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर चला गया, दूसरा ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढे और बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित किया।
कुषाण वंश के शासक-
भारत में कुषाण वंश का संस्थापक “कुलुज कडफिसेस” को माना जाता है। यह यूची कबीले का शक्तिशाली सरदार था। इसके नेतृत्व में यूची कबीला उत्तर के पर्वतों को पार हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया।
यहाँ इसने यूनानी राजा हरमोयम नामक व्यक्ति को हराकर काबुल तथा कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कुलुज कडफिसेस द्वारा जारी किये गये प्रारम्भिक सिक्कों में एक तरफ अन्तिम यूनानी राजा हरमोयम तथा दूसरी तरफ स्वयं उसकी आकृति खुदी हुई है।
बाद के सिक्कों में कुछ पर महाराजाधिराज, कुछ पर धर्मथिदस तथा कुछ पर धर्मथित खुदा हुआ मिलता है। कुलुज कडफिसेस ने केवल ताँबे के सिक्कें चलवाये। इसका शासन 15 ई. से 65 ई. तक माना जाता है।
विम कडफिसेस
कुलुज कडफिसेस की मृत्यु के बाद विम कडफिसेस गद्दी पर बैठा। चीनी ग्रन्थ हाऊ-हान-शू से पता चलता है कि इसने तक्षशिला और पंजाब क्षेत्र को विजित किया था। इस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सोने (सर्वप्रथम) और तांबे के सिक्के चलवाये।
भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों में एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि खुदी हुई है। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नन्दी एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि विम कडफिसेस शैव धर्म का उपासक था।
इसने महाराजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल 65 ई. से 78 ई. तक रहा।
कनिष्क
विम कडफिसेस के बाद कुषाण वंश की बागडोर कनिष्क के हाथों में आ गयी। कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे महान एवं योग्य शासक था।इसके काल में कुषाण शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ई. मानी जाती है। इसी वर्ष से शक सम्वत का प्रारम्भ माना जाता है।
कनिष्क ने पुरूषपुर (पेशावर) को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन पर थी। कनिष्क ने चीन के हन राजवंश के शासक पान चाओ को हराया था।
कनिष्क के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य-
1-चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन- कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुण्डलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान सम्प्रदायों में विभाजित हो गया।
इसी संगीति में महाविभाषा नामक पुस्तक का संकलन किया गया। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म का विश्वकोष भी कहा जाता है। इस पुस्तक में तीनों पिटकों पर लिखीं गयीं टीकाएँ संकलित है। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था।
2. गान्धार कला शैली-
गान्धार कला शैली का विकास कनिष्क के काल में गान्धार में हुआ। इसे इंडो-ग्रीक शैली या ग्रीक-बुद्धिष्ट शैली भी कहा जाता है। इस कला में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं।
3. मथुरा कला शैली-
इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस शैली में बौद्ध, हिन्दू एवं जैन धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय भी इसी शैली को जाता है।
4. सिल्क मार्ग पर अधिकार-
कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग की तीनों मुख्य शाखाओं पर अधिकार कर लिया था।कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, रूम सागर पर बने बन्दरगाह तक जाने वाला मार्ग, भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग।
5. विद्वानों को आश्रय-
कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। कनिष्क की राज्यसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित थी। जैसे-अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक आदि। बुद्धचरित, सौन्दरनन्द, शारिपुत्रप्रकरणम एवं सूत्रालंकार के रचनाकार अश्वघोष थे।
बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। नागार्जुन दार्शनिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी थे। इन्हें “भारत का आईन्सटाइन” कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया।
वसुमित्र ने बौद्ध धर्म के विश्वकोष महाविभाषा सूत्र की रचना की। चरक विद्वान एवं वैद्य था इसने चरक संहिता की रचना की।
6. कुषाण वंश के सिक्के-
सर्वप्रथम सर्वाधिक मात्रा में कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर उसे बलिदेवी पर बलि देते हुए दर्शाया गया है। कनिष्क के अब तक प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिले हैं। कुषाणों ने चाँदी के सिक्के नहीं चलाये।
कुषाण वंश का पतन
कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण वंश का पतन प्रारम्भ हो गया। कनिष्क के बाद उसका उत्तराधिकारी वासिष्क गद्दी पर बैठा। यह मथुरा और समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन करता था। इसके बाद क्रमशः हुविष्क, वासुदेव शासक हुए।
योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यमुना के तराई वाले भाग पर नाग लोगों ने अधिकार कर लिया। साकेत, प्रयाग एवं मगध को गुप्त राजाओं ने अपने अधिकार में कर लिया। नवीन राजवंशों के उदय ने भी कुषाणों के पतन में सहयोग दिया।
चालुक्य वंश ( Chalukya dynasty )
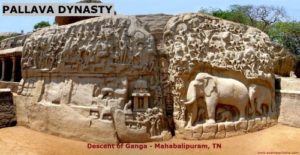
छठीं से आठवीं शताब्दी ईसवी तथा दस
वीं से बारहवीं शताब्दी ईसवी तक चालुक्य वंश दक्षिण में एक शक्तिशाली वंश था इन चालुक्य राजाओं की तीन शाखाएँ थीं-
- वातापि के चालुक्य।
- कल्याणी का उत्तरकालीन चालुक्य वंश।
- वेगी के पूर्वी चालुक्य वंश।
वातापि के चालुक्य ➖
पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। वह रणराज का पुत्र और जयसिंह का पौत्र था।
उसने वातापि (वादामी-बीजापुर जिले में) में दुर्ग बनवा कर इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने 535 ई. से 566 ई. तक राज्य किया। 567 ई. में कीर्तिवर्मा शासक हुआ।
कीर्तिवर्मा के पश्चात् उसका भाई मंगलेश गद्दी पर बैठा। मंगलेश और कीर्तिवर्मा के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ और मंगलेश मारा गया।
पुलकेशिन_द्वितीय
पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसका सबसे बड़ा कार्य उत्तर भारत के महान् सम्राट् हर्षवर्धन को पराजित करना था।
इस पराजय से हर्ष का राज्यविस्तार दक्षिण में बढ़ने से रुक गया और हर्ष की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा।
उसने गुर्जरों को भी हराया तथा कलिंग और गुजरात को भी कर देने पर विवश किया। परन्तु पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा नरसिंह वर्मा ने तीन युद्धों में पराजित किया और अन्तिम युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय वीरगति को प्राप्त हुआ।
पुलकेशिन द्वितीय के बाद भी कई प्रसिद्ध राजा हुए जिनमें विकम्रादित्य प्रथम (655-681 ई.), विक्रमादित्य द्वितीय (734-757 ई.) उल्लेखनीय हैं। इनका पल्लवों से युद्ध चलता रहा। कीर्तिवर्मा द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग ने पराजित कर दिया और चालुक्यों के राज्य पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया।
कल्याणी का उत्तरकालीन चालुक्य वंश-
इस वंश का प्रथम शासक तैल या तैलप द्वितीय (973-997 ई.) था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी।इसने चालुक्य वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित किया। अगले शासक सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से हटाकर कल्याणी को बनाया और इसी से यह वंश कल्याणी का चालुक्य वंश कहलाया।
इसने अपने राज्य का विस्तार किया। कौशल और कलिंग इसके राज्य में शामिल थे। चोल राजा राजेन्द्र द्वितीय ने इसे युद्ध में पराजित किया। अत: उसने 1068 ई. में करूवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर महायोग को प्राप्त किया।
विक्रमादित्य षष्ठ और सोमेश्वर तृतीय अन्य शासक हुए। विक्रमादित्य ने शक संवत् का प्रयोग बंद करके विक्रम चालुक्य संवत शुरू किया।इसके दरबार में विल्हण ने विक्रमांकदेवचरित् की रचना की। मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर उसी के दरबार में रहता था।
सोमेश्वर तृतीय के समय होयसल शासक विष्णुवर्द्धन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसने अभिलाषीतार्थ चिन्तामणि या मनसोल्लास की रचना की। अत: इसे सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। तैलप तृतीय इस वंश का अन्तिम शासक था जिसे उसके सेनापति बिज्जल ने हराकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया।
प्रान्तीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और चालुक्य राज्य के स्थान पर होयसल, यादव तथा काकतीय तीन वंशों ने क्रमशः द्वारसमुद्र, देवगिरि तथा वारंगल में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किये।
वेंगी का पूर्वी चालुक्य वंश-
पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसने 615 से 633 ई. तक राज्य किया इसकी राजधानी वेंगी थी। इसके पश्चात् जयसिंह प्रथम (633-663 ई.), इन्द्रवर्मा (केवल एक सप्ताह) और विष्णुवर्धन द्वितीय (663-672 ई.) राजा बने।
विष्णुवर्धन द्वितीय के पुत्र मेगी युवराज ने (672-696 ई.) तक राज्य किया। जयसिंह द्वितीय (696-709 ई.) उसका उत्तराधिकारी बना। उसके बाद उसका छोटा भाई कोकुलि विक्रमादित्य शासक बना। उसे परास्त कर उसके बड़े-भाई विष्णुवर्धन तृतीय (709-746 ई.) ने राज्य किया।
अन्य शासक विजयादित्य प्रथम (746-764 ई.), विजयादित्य द्वितीय (799-843 ई.), विजयादित्य तृतीय (844-888 ई.), भीम प्रथम (888-918 ई.), भीम तृतीय (934-945 ई.), विक्रमादित्य षष्ठ (948-970 ई.) हुए। 973 से 1003 ई. तक पूर्वी चालुक्यों के राज्य का प्रशासन सम्भवत: चोलों ने चलाया।
इसके पश्चात् शक्तिवर्मा (1003-1015 ई.), विष्णुवर्धन अष्टम (1020-1063 ई.) और कुलोत्तुंग चोलदेव (1063-1118 ई.) शासक हुए।
धर्म और कला
चालुक्य नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उनके शासन-काल में पौराणिक देवताओं की पूजा का प्रचलन बढ़ा। इन नरेशों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया। पूजा में यज्ञों की प्रथा को बढ़ावा मिला। पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेघ यज्ञ किया।
उसके दरबार में कवि रविकीर्ति था जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना की। रविकीर्ति ने जिनेन्द्र का मंदिर बनवाया। यद्यपि चालुक्य राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, परन्तु वे धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण दक्षिण में जैन-धर्म को भी प्रोत्साहन मिला।
विक्रमादित्य द्वितीय ने जैन-धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। चालुक्यों के शासन-काल में कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। चट्टानों को काटकर विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया गया। अजन्ता और एलोरा दोनो चालुक्य राज्य में स्थित थे। अजन्ता के कुछ भित्तिचित्र चालुक्य काल के थे।
एलोरा में चट्टानों को काटकर बने कुछ मन्दिर चालुक्य स्थापत्य कला की याद दिलाते हैं, जैसे कैलाश पर्वत के नीचे रावण, नृत्य करते हुए भगवान् शिव और नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दिखाये गये हैं।
ऐहोल के विष्णु मन्दिर में विक्रमादित्य द्वितीय का एक अभिलेख सुरक्षित है। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी ने पट्टत्कल में लोकेश्वर नाम से एक शिव मन्दिर का निर्माण कराया जो विरुपाक्ष मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार चालुक्यों के शासन काल में स्थापत्य कला को विशेष प्रोत्साहन मिला।
चालुक्य शासकों के समय के भित्तिचित्रों में महत्त्वपूर्ण वह चित्र है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत का स्वागत करते दिखलाया गया है।
हिन्द यवन वंश
यूनानी शासन (ईसा पूर्व) :

यूनानियों ने भारत के पश्चिमी छोर के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया। बौद्धकाल में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। यूनानियों ने सबसे पहले इसी आर्याना क्षेत्र पर आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों को अपने अधीन ले लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा।
इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से जाना जाता है। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली सिकंदर (356 ईपू) था जिसे उसके देश में अलेक्जेंडर और भारत में अलक्षेन्द्र कहा जाता था। सिकंदर ने अफगानिस्तान एवं उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था।
बाद में इस भाग पर उसके सेनापति सेल्यूकस ने शासन किया। हालांकि सेल्यूकस को ये भू-भाग चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित कर देने पड़े थे। बाद के एक शासक डेमेट्रियस प्रथम (ईपू 220-175) ने भारत पर आक्रमण किया। ईपू 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाया।
युक्रेटीदस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस का अधिकार पूर्वी पंजाब और सिन्ध पर भी था। भारत में यवन साम्राज्य के दो कुल थे- पहला डेमेट्रियस और दूसरा युक्रेटीदस के वंशज।
मीनेंडर (ईपू 160-120) :
यह संभवतः डेमेट्रियस के कुल का था। जब भारत में नौवां मौर्य शासक वृहद्रथ राज कर रहा था, तब ग्रीक राजा मीनेंडर अपने सहयोगी डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ युद्ध करता हुआ सिन्धु नदी के पास तक पहुंच चुका था।
सिन्धु के पार उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस मीनेंडर या मिनिंदर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। हालांकि बाद में मीनेंडर ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। मिलिंद पंजाब पर राज्य करने वाले यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा था।
उसने अपनी सीमा का स्वात घाटी से मथुरा तक विस्तार कर लिया था। वह पाटलीपुत्र पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया।
राष्ट्रकूट एवं पाल वंश
राष्ट्रकूट वंश का आरम्भ ‘दन्तिदुर्ग’ से लगभग 736 ई. में हुआ था। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इसके उपरान्त इन शासकों ने मान्य खेत, (आधुनिक मालखंड) को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों ने 736 ई. से 973 ई. तक राज्य किया।
शासन तन्त्र राष्ट्र कूटों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया था। प्रशासन राज तन्त्रात्मक था।राजा सर्वोच्च शक्तिमान था।राजपद आनुवंशिक होता था। शासन संचालन के लिए सम्पूर्ण राज्य को राष्ट्रों, विषयों, भूक्तियों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था।
राष्ट्र, जिसे ‘मण्डल’ कहा जाता था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ‘ग्राम’ थी। राष्ट्र के प्रधान को ‘राष्ट्रपति’ या ‘राष्ट्रकूट’ कहा जाता था।
एक राष्ट्र चार या पाँच ज़िलों के बराबर होता था। राष्ट्र कई विषयों एवं ज़िलों में विभाजित था। एक विषय में 2000 गाँव होते थे। विषय का प्रधान ‘विषयपति’ कहलाता था। विषयपति की सहायता के लिए ‘विषय महत्तर’ होते थे। विषय को ग्रामों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था।
प्रत्येक भुक्ति में लगभग 100 से 500 गाँव होते थे। ये आधुनिक तहसील की तरह थे। भुक्ति के प्रधान को ‘भोगपति’ या ‘भोगिक’ कहा जाता था।
इसका पद आनुवांशिक होता था। वेतन के बदले इन्हें करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। भुक्ति छोटे-छोटे गाँव में बाँट दिया गया था, जिनमें 10 से 30 गाँव होते थे। नगर का अधिकारी ‘नगरपति’ कहलाता था।प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी।
ग्राम के अधिकारी को ‘ग्रामकूट’, ‘ग्रामपति’, ‘गावुण्ड’ आदि नामों से पुकारा जाता था। इसकी एक ग्राम सभा भी थी,जिसमें ग्राम के प्रत्येक परिवार का सदस्य होता था।
गाँव के झगड़े का निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य था।
पाल वंश

पाल साम्राज्य मध्य कालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासन था जो कि 750-1174 इसवी तक चला। पाल राज वंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तु कला को बहुत बढावा मिला। पाल राजा बौद्ध थे।यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था।
जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गहरा संकट उत्पन६न हो गया, तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकत फैली थी। इसी समय गोपाल ने बंगाल में एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया।
जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया था। वह योग्य और कुशल शासक था, जिसने 750 ई. से 770 ई. तक शासन किया इस दौरान उसने औदंतपुरी (बिहार शरीफ) में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। आठवीं सदी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ।
गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। धर्मपाल ( 770-810 ई.) गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ई. में सिंहासन पर बैठा।धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया।धर्मपाल ने कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा रहा।
उसने कन्नौज की गद्दी से इंद्रायूध को हराकर चक्रायुध को आसीन किया। देवपाल (810-850 ई.)धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था।
शक वंश

प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का अन्त हो गया और उसके स्थान पर मध्य एशिया की शक जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। शक वंश के उद्भव का इतिहास बड़ा प्राचीन है। द्वितीय शती ईसा पूर्व में संभवत: काफिरिस्तान तथा हजारा क्षेत्र में शकों का राज्य था।
फारस के राजा डेरियस (522-486 ई.पू.) के समय शक लोग सोग्डियन के बाहर संभवत: जरसेक्स (जरजेस) या सीर दरिया के मैदानी इलाके में निवास करते थे किंतु प्रथम शती ई.पू. के अन्तिम दशकों में सीगल (सीस्तान) के निवासी बस गये।
रैप्सन ने शकों के निवास-स्थान के विषय में तीन स्थापनाएँ की हैं। हेरोडोटस के कथन के आधार पर इन्हें बैक्ट्रियनों का पड़ोसी कहा जा सकता है। दूसरा स्थान फारस या पर्सिया के ड्रेगनियना क्षेत्र में हेलमड नदी के किनारे आधुनिक सीस्तान हो सकता है जिसे शकों का निवास या शकस्तान भी कहा है।
तीसरे मत के अनुसार ये लोग समुद्र के किनारे काले सागर के उत्तर में रूसी साम्राज्य के समीप में, बैक्ट्रियन प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते थे।
भारत में शक सिथियन के नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ ग्रंथों में उनके लिए शक-पह्लव शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि संभवत: शक और पार्थियन एक ही समूह से संबद्ध थे। माना जाता है कि शक बोलन दरें के रास्ते से भारत आए और निचले सिंधु क्षेत्र में स्थापित हो गए।
शकों की पाँच शाखाएँ भारत में शासन करती रहीं।
- पहली शाखा अफगानिस्तान में स्थापित थी।
- दूसरी शाखा पंजाब में स्थापित हुई और तक्षशिला उसकी राजधानी हुई।
- तीसरी शाखा मथुरा में स्थापित हो गई।
- चौथी शाखा पश्चिम भारत में स्थापित हुई, जो चौथी सदी तक शासन करती रही।
- पाँचवीं शाखा उत्तरी दक्कन में स्थापित हुई।
यूनानी, रोमन और चीनी वृत्तान्त से शकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय ग्रंथों में पतंजलि के महाभाष्य से भी इसके बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुराणों एवं महाकाव्यों से भी इन पर कुछ प्रकाश पड़ता है।
प्रथम शक शासक मोगा या माऊस था। उसका उत्तराधिकारी एजेय था। इसने अन्तिम ग्रीक शासक हेसाट्रेटस को भारत से खदेड़ दिया।पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण शासक रूद्रामन (130 ई.150 ई.) था। वह दो कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध है- (1) उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसका व्यय उसने व्यक्तिगत कोष से दिया, (2) दूसरे, उसने संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख लिखवाया। यह जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है।
उज्जैन का प्रथम स्वतंत्र शासक चष्टन था।माना जाता है कि मालवा के एक भारतीय शासक ने 58 ई.पू. में एक शक शासक को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रम संवत चलाया, जो 57 ई.पू. से शुरू होता है। माना जाता है कि भारत में अभी तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं।
प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश प्राचीन प्रमुख राजवंश

